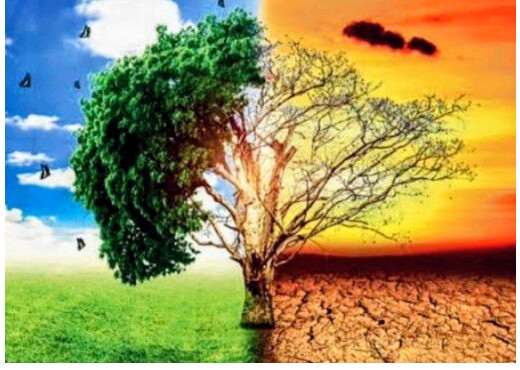सार्वकालिक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई
- Post By Admin on Aug 24 2024

किसी भी महान लेखक को तत्कालीन समय, समाज, परिस्थितियां और उनसे निर्मित झंझावात गढ़ता है । जब तमाम तरह की विसंगतियों एवं तपिश में तपकर वह बाहर निकलता है तब वह निडर, निष्पक्ष , ठोस एवं सार्वकालिक लोक शिक्षक की भूमिका में आ जाता है । व्यंग्य शिरोमणि हरिशंकर परसाई के व्यंग्यकार का निर्माण भी कुछ उन्हीं परिस्थितियों में हुआ । यही कारण है कि प्रेमचंद की तरह परसाई की रचनाएं भी पाठकों के भीतर उतरकर उसकी आत्मा से सीधा संवाद करती हुई उसे पूरी तरह झकझोरती एवं बेचैन कर देती है। आज जैसे - जैसे जीवन अपनी रफ़्तार तीव्र से तीव्रतर करता जा रहा है , वैसे-वैसे उस रफ्तार में जिंदगी पीछे छूटती जा रही है । जैसे -जैसे जीवन जीने की शर्तें कठिन से और अधिक कठिन होती जा रही हैं वैसे- वैसे परसाई की रचनाएं पहले से और अधिक प्रासंगिक और मारक प्रतीत होती है।
परसाई के व्यंग्य को पढ़ते हुए पाठक खुद को सहज ही साधारणीकृत कर लेता है। उनकी रचनाओं में यह विशेषता इसलिए समाहित हो सकी , क्योंकि जीवन की विद्रूपताओं को परसाई ने झेला और भोगा है । 22 अगस्त 1922 ई. को मध्यप्रदेश के सतपुड़ा की तलहटी में नर्मदा के तट पर बसे गांव में पिता झूमकलाल के घर में जन्मे परसाई ने बालपन में ही भयंकर प्लेग में क्रमशः मां और कुछ वर्षों के उपरांत पिता को खो दिया । तबसे वह खुद को नर्मदापुत्र कहते आए हैं। पिता झूमकलाल ने बचपन में ही उन्हें रामचरित मानस का इतनी बार पाठ कराया कि उसके दोहे - चौपाइयां सब इन्हें कंठस्थ हो गए थे । पिता के बाद सबसे अधिक प्रभावित वह अपने एक अध्यापक 'बग्गा साहब' से हुए। परसाई ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि " बग्गा साहब ने ही मुझे साहित्य के संस्कार दिए और ज्ञान की अनंत पिपासा दी। उन्होंने मुझे इतिहास चेतना दी और इतिहास बोध दिया। ( वसुधा -41 , पृष्ठ 132)
पिता के जाने के बाद घर का सारा बोझ परसाई के कंधे पर। मन अशांत । उस अभाव से उबरने एवं दायित्व निर्वहन की बेचैनी । खंडवा में अध्यापन कार्य शुरू । छ: महीने बाद 1942 ई. में जबलपुर अध्यापन -प्रशिक्षण हेतु प्रस्थान। उनकी आर्थिक तंगी की भयावहता को कांति कुमार जैन ने परसाई की खंडवा से जबलपुर की इस यात्रा का वर्णन इन शब्दों में किया है - " यह यात्रा विदाउट टिकट थी.... पर भूख तो लगती ही है सो जब भी स्टेशन आता , मास्साब ( परसाई) नीचे उतरते , नल पर जाकर भरपेट पानी पीते और अगले स्टेशन तक के लिए भूख को ठेंगा दिखाते रहते।"( तुम्हारा परसाई, पृष्ठ 48)
परसाई के व्यंग्यकार का विकास उनकी अपनी समस्याओं और उनके समाधान के संघर्षों के क्रम में हुआ। इसी क्रम में उन्हें सदाशयी, शुभचिंतक, पाखंडी, ईमानदार, छद्म नेता, छुटभइये, सामान्य लोग, मित्र और शत्रु मिले। उनके व्यंग्य में जो करुणा बहती है, उसका मूल कारण उनका आत्म संघर्ष है। उनका संपूर्ण व्यंग्य साहित्य स्वातंत्र्योत्तर भारत की आशा निराशा, मोहभंग के द्वंद्व का दस्तावेज है। उनकी संवेदना में आत्मसंघर्ष और युग संघर्ष का अद्भुत मेल है।
जीवन का कोई भी क्षेत्र परसाई के व्यंग्य से बच न सका चाहे वह राजनीति हो या समाज हो, धर्म हो या दर्शन, कुत्ता हो या गाय, भिक्षा हो या शिक्षा , रिटायरमेंट के उपरांत पेंशन हेतु सचिवालय का चक्कर हो या डाक्ट्रेट के लिए 'रीसर्च का चक्कर' सभी विषयों व समस्याओं की पटरी पर उनके व्यंग्य की रेल बेधड़क दौड़ी। उनका 'रीसर्च के चक्कर' नामक व्यंग्य विश्वविद्यालय में व्याप्त गुटबाजी, जातिवाद, शैक्षणिक अराजकता आदि की परतों को अनावृत करता है । इसमें रीसर्च को परिभाषित करते हुए लिखते हैं -"एम.ए. करने से नौकरी मिलने तक जो काम किया जाता है, उसे रीसर्च कहते हैं। वह दफ्तर जाने से पहले किया गया हरि स्मरण है। इसलिए अधिकांश शोध प्रबंध विष्णुसहस्त्रनाम है - यानी उनमें एक ही बात हजार तरीके से कही जाती है। "
जाति भारतीय समाज की एक विकृत सच्चाई है जो लेखक के इस व्यंग्य में भी दिखाई दे जाती है । शोधपूर्व वार्तालाप में आचार्य जी का परसाई से पहला प्रश्न यही पूछा गया -".. अच्छा पहले यह बताओ, तुम कौन जात हो?"और इसी वार्तालाप से जो चीजें निकलती हैं, उससे संस्थानगत गुटबाजी, जातिवाद आदि के जाल में जकड़ी हुई शिक्षा और घुट रही प्रतिभा और पीछे छूट चूकी भारतीय संस्कृति हमारे सामने हमसे हिसाब मांगती हुई प्रतीत होती है! आगे आचार्य जी कहते हैं -"....तुम रिसर्च शुरू करो। पर पहले रिसर्च का अर्थ समझ लो। इसका अर्थ है - फिर से खोजना यानी जो पहले ही खोजा जा चुका है, उसे फिर से खोजना रिसर्च कहलाता है।... भारत के विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसरान हमारे विरोधी हैं उनके ग्रंथों और निष्कर्षों को तुम्हें नहीं देखना है, क्योंकि तब तुम्हारा काम रिसर्च न होकर सर्च हो जाएगा ।" .... आचार्य जी ने फिर तमाम शोधार्थियों को शोध कार्य आवंटित करते हुए कहा -"तुम जानते हो कि अभी इस राज्य में मुख्यमंत्री बदला है। तुम्हें एक सप्ताह में शोध करना है कि इसका विश्वविद्यालय पर क्या असर पड़ेगा। पूरी तरह पता लगाओ कि किस अध्यापक के उनसे कैसे संबंध हैं?... उपकुलपति उनके कृपापात्र हैं कि नहीं?और वे किन बातों से खुश होते हैं? देखो,इस विषय पर बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि इसी पर तुम्हारे थिसिस की योग्यता निर्भर है!" आज हमारे देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जो शोध कार्य के साथ संगीन मजाक चल रहा है उसका परसाई जी का यह व्यंग्य सभी परतों को अनावृत करता है ।
उनके व्यंग्य की यही सार्वकालिकता उन्हें प्रेमचंद के योग्य उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करती है। प्रेमचंद ने जहां स्वतंत्रता पूर्व के भारतीय जनमानस व जीवन की तमाम बेचैनियों का उद्घाटन किया वहीं परसाई ने उनकी उस परंपरा को अपने व्यंग्य के माध्यम से अभूतपूर्व व्याप्ति दी है। उसमें नई स्थितियों का समावेश करने के साथ साथ समकालीन भारत की व्यापक महागाथा लिखी है। वे सही मायने में प्रेमचंद के ऐसे उत्तराधिकारी लेखक हैं, जिन्हें स्वातंत्र्योत्तर भारत की ऐतिहासिक विसंगति, मोहभंग और क्षोभ का लेखक कहा जाता है। उनके व्यंग्य का यही मिजाज उन्हें सार्वभौमिक व सार्वकालिक लोकशिक्षक बनाता है ।
(डॉ. सुधांशु कुमार : लेखक व्यंग्यकार, स्तंभकार एवं शिक्षाविद हैं)


.jpg)